ग़ुलाम हैदर उन महत्वपूर्ण और अग्रणी फ़िल्म संगीतकारों में से थे जिन्होंने फ़िल्म म्यूजिक को राह दिखाई। उनमें गायकों की प्रतिभा को पहचानने और तराशने की अद्भुत क्षमता थी।
ग़ुलाम हैदर ने करियर की शुरुआत दन्त चिकित्सक के रूप में की
मास्टर ग़ुलाम हैदर का जन्म 1908 में हैदराबाद सिंध में हुआ। उनके पूर्वज अमृतसर के रब्बी थे और संगीत उनके खून में था, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो संगीत को पेशा बनाएँ। इसीलिए उन्होंने दो साल तक बतौर डेंटिस्ट प्रैक्टिस की यानी वो मुख्य रूप से दन्त चिकित्सक थे, लेकिन डेंटिस्ट्री में उनका मन नहीं रहा था। थिएटर और म्यूज़िक में उनकी गहरी रुचि थी, शुरुआत में उन्होंने बीबे ख़ान से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली।
कृपया इन्हें भी पढ़ें – ज्ञानदत्त ने अपने वक़्त में एक से बढ़कर एक हिट गीत दिए पर उनका अंत भी गुमनामी में ही हुआ
उन्होंने हरिदासजी से हारमोनियम और भाई मेहर बख्श से तबला सीखना शुरू किया। फिर उन्होंने बाबू गणेशलाल से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और डेंटिस्ट्री छोड़कर पूरी तरह थिएटर और संगीत में ही रम गए। उस समय कोलकाता फ़िल्म निर्माण का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, तो ग़ुलाम हैदर भी कोलकाता पहुँच गए। उन्होंने अल्फ़्रेड थिएटर कंपनी और एलेक्ज़ेंडर थिएट्रिकल कंपनी में बतौर पियानो प्लेयर काम किया।

संगीत के सफ़र की शुरुआत हुई थिएटर से
लेकिन सिर्फ़ वादक बनने से वो संतुष्ट नहीं थे इसलिए वापस लाहौर लौट आये और वहाँ जेनोफोन रिकॉर्डिंग कंपनी में संगीत निर्देशक के रूप में काम करने लगे। ये रिकॉर्डिंग कंपनी पंजाबी और उर्दू में फिल्मी और ग़ैर-फिल्मी रिकॉर्ड बनाती थी। तो फ़िल्मों में ग़ुलाम हैदर की शुरुआत भी यहीं से हुई। पंजाबी फ़िल्म स्वर्ग की सीढ़ी (1935) और मजनूँ (1935) के लिए उन्होंने संगीत दिया।
फ़िल्म “स्वर्ग की सीढ़ी” की हेरोइन थीं “उमराव ज़िया बेगम” जो उस समय की प्रसिद्ध गायिका भी थीं। वो पंचोली पिक्चर्स में काम करती थीं, उनके लिए ग़ुलाम हैदर ने काफ़ी गाने कंपोज़ किये और बाद में उन्हीं से उनकी शादी हुई। ग़ुलाम हैदर की पहली हिट फ़िल्म आई 1939 में पंचोली पिक्चर्स के साथ, “गुलबकावली” इसमें नूरजहाँ के गाए गाने बहुत मशहूर हुए।
ग़ुलाम हैदर ने कई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया
नूरजहाँ जब 9-10 साल की थीं जब वो ग़ुलाम हैदर से मिलीं थीं। पंचोली स्टूडियो में जब नूरजहाँ ने उन्हें एक गाना सुनाया “प्यारे रसिया बिहारी बिनती सुनो हमारी”, उनकी क़ाबिलियत देखकर ग़ुलाम हैदर ने उनसे क्लासिकल गाने गवाए। उन्हीं की शागिर्दी में नूरजहाँ ने प्लेबैक के गुर सीखे, माइक पर कैसे खड़े होना है, गाते हुए बोल गिनना, सब उन्हीं से सीखा। इसके बाद आई “यमला जट” में भी नूरजहाँ ने क्लासिकल गाने गाए।

उस समय लाहौर फ़िल्म इंडस्ट्री में तीन मुख्य फ़िल्मकार थे – आर के शोरी, ए आर कारदार, और दलसुख पंचोली और इन तीनों ही फ़िल्म कंपनियों के साथ मास्टर ग़ुलाम हैदर मुख्य रूप से काम कर रहे थे। उस वक़्त तक उनका काफ़ी नाम हो चुका था लेकिन उनकी तब तक की सबसे बड़ी हिट रही “ख़ज़ांची” जो 1941 में आई थी। इस फिल्म का संगीत एक तरह की क्रांति लेकर आया, जो उस दौर की ज़्यादातर फ़िल्मों की तरह राग-रागिनियों में नहीं बंधा था।
कृपया इन्हें भी पढ़ें – रामचंद्र पाल प्रतिष्ठित स्टूडियो के गुमनाम संगीतकार
इस संगीत में एक ताज़गी थी, एक खुलापन था जिसने बाद में कई और संगीतकारों को प्रेरित किया। ख़ज़ांची का एक गाना “सावन के नज़ारे हैं” तो बहुत ही मशहूर हुआ था। इसे गाया था शमशाद बेगम ने, जिन्हें गायन की दुनिया में लाने का श्रेय भी मास्टर ग़ुलाम हैदर को ही जाता है। उन्होंने ही शमशाद बेगम की क़ाबिलियत को पहचाना और 13 साल की शमशाद बेगम से एक पंजाबी नॉन-फ़िल्मी गाना रिकॉर्ड कराया।

वो गाना बहुत हिट हुआ और इसके बाद तो शमशाद बेगम ने जेनोफोन कंपनी के लिए साल भर में क़रीब 200 गाने रिकॉर्ड किए। साथ ही फ़िल्मों में भी शुरुआत हो गई और “ख़ज़ांची” फ़िल्म से वो हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में पूरी तरह स्थापित हो गईं। ख़ज़ांची का म्यूज़िक इतना पॉपुलर हुआ कि उसके बाद उसकी लोकप्रियता को भुनाते हुए “ख़ज़ांची” नाम से नई प्रतिभाओं की तलाश में एक कॉम्पिटिशन शुरु हुआ जिसमें छोटी लता मंगेशकर ने भी भाग लिया और उसे जीता भी।
वो मास्टर ग़ुलाम हैदर ही थे जिन्होंने लता मंगेशकर की प्रतिभा पर सबसे पहले न सिर्फ़ विश्वास जताया था, बल्कि उनकी कामयाबी की भविष्यवाणी भी की थी। इनके अलावा सुधा मल्होत्रा, सुरिंदर कौर जैसी गायिकाओं की प्रतिभा को सामने लाने और उसे निखारने का काम भी ग़ुलाम हैदर ने ही किया। “खज़ांची” के बाद आई एक और बड़ी हिट “ख़ानदान” जिसमें डी एन मधोक का लिखा और नूरजहाँ का गाया ये गाना “तू कौन सी बदली में मेरे चाँद है आजा” आज भी पॉपुलर है।
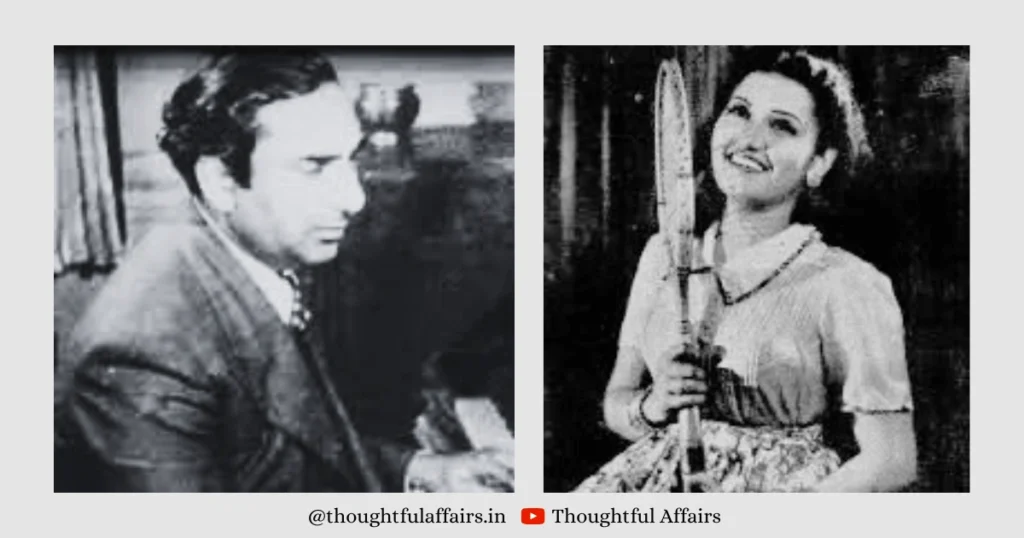
सबसे ज़्यादा मेहनताना पाने वाले पहले संगीतकार
इसके बाद ग़ुलाम हैदर ने “जमींदार” और “पूँजी” जैसी कुछ फ़िल्में की। तब तक उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें मुंबई से भी ऑफर आने शुरु हो गए थे। के. आसिफ़ ने उन्हें 25000 रुपए की ऑफर दी थी अपनी फ़िल्म “फूल” में संगीत देने के लिए, पर इस फिल्म की रिलीज़ से पहले ग़ुलाम हैदर की कुछ और फिल्में रिलीज़ हो गईं। इनमें फ़िल्मिस्तान की 1944 में आई “चल चल रे नौजवान” और महबूब प्रोडक्शंस की 1945 में आई “हुमायूँ” भी शामिल है।
कहते हैं “हुमायूँ” में संगीत देने के लिए मास्टर ग़ुलाम हैदर ने 50000 फ़ीस ली थी। इससे पहले संगीतकारों को इतना मेहनताना नहीं दिया जाता था। इस तरह उन्होंने संगीतकारों की अहमियत को बढ़ाया और उन्होंने ही फ़िल्म संगीतकारों की एसोसिएशन बनाने की पहल भी की। मुंबई में भी मास्टर ग़ुलाम हैदर ने बैरम खाँ(46), शमाँ(46), मँझधार(47), मेहँदी(47), पतझड़(48), बरसात की एक रात(48) जैसी फ़िल्मों में संगीत दिया और अपनी क़ाबिलियत का लोहा मनवाया, उनकी गिनती इंडस्ट्री के दिग्गजों में होने लगी।
ग़ुलाम हैदर ने लता मंगेशकर की कामयाबी की भविष्यवाणी की थी
उन्हीं दिनों की बात है जब वो लता मंगेशकर की गायकी से प्रभावित होकर उन्हें लेकर फिल्मिस्तान पहुँचे ताकि ‘शहीद” फ़िल्म में उनका एक गाना रख सकें। मगर उस ज़माने में थोड़ी नेज़ल और भारी आवाज़ों का चलन था। जब शशधर मुख़र्जी ने लता मंगेशकर की आवाज़ को सुना तो ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये आवाज़ बहुत पतली है फ़िल्म की हेरोइन को सूट नहीं करेगी, ये आवाज़ चल ही नहीं सकती। इस बात पर मास्टर ग़ुलाम हैदर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा – मुखर्जी साहब ये आवाज़ चलेगी ही नहीं दौड़ेगी और ऐसा दौड़ेगी एक दिन आप सब लोग इसके पीछे-पीछे दौड़ेंगे।
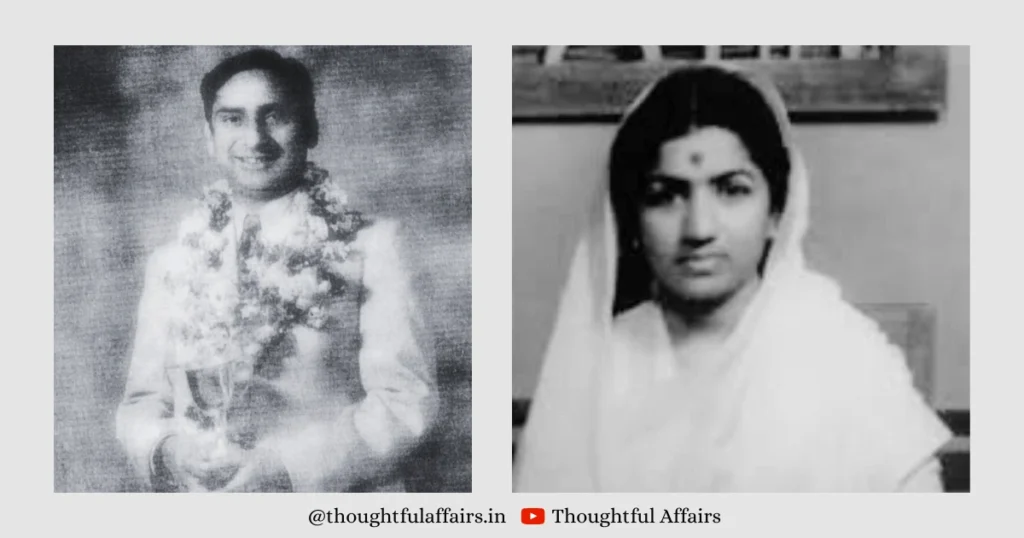
और ग़ुलाम हैदर लता मंगेशकर को लेकर वहाँ से निकल गए। स्टेशन पर ट्रैन का इंतज़ार करते हुए उन्होंने एक धुन बनाई और वहीं लता मंगेशकर ने उस धुन पर गुनगुनाना शुरु किया। और फिर वो गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में उसी दिल बॉम्बे टॉकीज़ की फ़िल्म “मजबूर” के लिए रिकॉर्ड हुआ। मजबूर के गाने काफ़ी मशहूर हुए साथ ही “शहीद” के गीतों ने भी बहुत लोकप्रियत पाई। कहते हैं वो बिला वजह दाद नहीं देते थे, उनका मानना था कि जब तक दिल से वाह न निकले दाद का कोई मतलब नहीं है।
कृपया इन्हें भी पढ़ें – चित्रगुप्त – सुरों का लेखा-जोखा रखने वाले संगीतकार
विभाजन के बाद बहुत से और फ़नकारों की तरह ग़ुलाम हैदर भी पाकिस्तान चले गए। मुंबई में एक तरह से 1949 की “कनीज़” ही उनकी आखिरी महत्वपूर्ण फिल्म रही हाँलाकि इसके भी सभी गीत पूरे नहीं हुए थे और बाक़ी गीतों की धुनें हंसराज बहल ने बनाई। इसके अलावा “पुतली”, “आबशार” जैसी उनकी कई फिल्में अधूरी रह गई उनकी धुनें भी दूसरे संगीतकारों ने बनाईं।
1935 से 1953 तक 18 साल के अपने फ़िल्मी सफ़र में उन्होंने लगभग 32 फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें पंजाबी फिल्में भी शामिल हैं। पाकिस्तान में भी उन्होंने संगीत देना जारी रखा, उनके संगीत निर्देशन में आई कुछ आख़िरी फिल्में थीं “गुलनार ” और “लैला”। वो शायद और बेहतर म्यूज़िक देते मगर कैंसर ने उनकी ज़िंदगी बहुत कम कर दी और 9 नवम्बर 1953 में सिर्फ़ 45 साल की उम्र में वो इस दुनिया से रुख़्सत हो गए।
ग़ुलाम हैदर का नाम उन संगीतकारों में शामिल किया जाता है जिन्होंने फ़िल्म संगीत का रुख़ बदला और कई प्रतिभाओं का परिचय फ़िल्म इंडस्ट्री से कराया। उनका नाम और काम किसी परिचय का मोहताज नहीं है और जब तक उनका संगीत रहेगा उनका नाम भी फिल्म इतिहास में अमर रहेगा।
